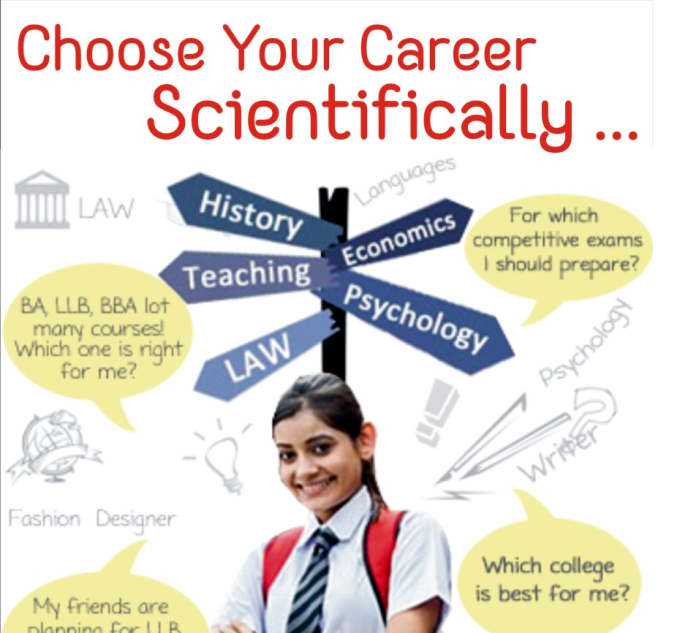आज हर मां-बाप शिक्षा को स्तरहीन बना रहे है, कुछ ही है जो बच्चों को रूचिनुसार शिक्षा दिला पाने में सफल हो पाते है I अधिकतर माँ-बाप अपनी बुद्धि को ही आधार मान-कर बच्चों को अपने विवेक के अनुसार विषय दिलाकर उस पर पूर्ण ध्यान केन्द्रित करने का दबाब बनाते है I आज समाज में प्रतिष्ठित बनने की होड़ मची होने के कारण कोई भी अपने बच्चो को दबाव-मुक्त शिक्षा नही दे पा रहे है, और उसका परिणाम ???? बस छात्र भटकाव की ओर अग्रसर हो जाता है I दबाव में रहने वाला हर विद्यार्थी जैसे-तैसे डिग्री पास कर अपने योग्यतानुसार सही क्षेत्र में कार्य ना मिलने के कारण, वह तय नहीं कर पाता की उसका महत्त्व डिग्री के उपरांत परिवार एवं समाज में कैसे मिले?? दूसरी तरफ उम्र बढ़ते रहने के कारण उसे जो भी क्षेत्र मिलता है उसमें अपनी आजीविका शुरू कर अपने सही रूप को भूलकर बनावटी सामाजिक परिवेश को अपनाता है | आज ९०% छात्रों ने अपना जीवन इसी तरह किसी न किसी अनचाहे क्षेत्र में सिर्फ जीविका के आधार पर चुना है I ९० से १००% अंक लाने वाले छात्र भी अपने अनुसार जीवन नही बना पाते है, तथा उनका आई.क्यू बढ़िया होने के बाबजूद भी वो अपने शिक्षा को वास्तविक स्वरुप नही दे पाते है I अतः अब हमे छात्रों के मानसिक क्षमता पर आधारित शिक्षा को ही महत्त्व देना चाहिए I
जानवरों की तरह बच्चों के पीछे पड़ने से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है| इसलिए शिक्षा का स्वरुप बच्चो के दिमागी क्षमाताओ के अनुसार होना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियों को अपने सही दिशा की ओर अधिक से अधिक बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें| शिक्षा प्राप्त करने पर सुविधा प्राप्त होती है तथा में प्रसन्नचित्त होने के कारण जो भी शिक्षा ग्रहण करता है, वह उसके भावी जीवन को प्रसन्नचित्त रखकर जीने का अधिकार देती है| इस तरह विद्यार्थी में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता तथा छात्र एवं पालको के मध्य सामंजस्य होने के कारण शिक्षा का भावी रूप दिखाई देने लगता है I
मित्रो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को एक नयी विचारधारा, नया सवेरा देता है, ये हमे एक परिपक्व समाज और स्वर्णिम राष्ट्र बनाने में मदद करता है । यदि शिक्षा के उद्देश्य सही दिशा मे हों तो ये इन्सान को नये नये प्रयोग करने के लिये उत्साहित करते हैं । शिक्षा और संस्कार साथ साथ चलते हैं, या कहा जाये तो एक दूसरे के पूरक हैं । शिक्षा हमें संस्कारों को समझने और बदलती सामाजिक परिस्थियों के अनुरूप उनका अनुसरण करने की समझ देता है । आज शिक्षा जिस मुकाम पर पहुँच चुकी है वहाँ उसमें परिवर्तन की गुंन्जाइश है, आज हमें मिल बैठकर सोचना चाहिये, कि यदि शिक्षा हमारे उद्देश्यों को पूरा नही करती तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है ।
कैरियर के चुनाव मे उधेड़बुन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। फैसला बिल्कुल अपने लक्ष्य को केन्द्र में लेकर होना चाहिए। यदि आई.ए.एस. बनना है तो अपको किस रूचि के विषय को अपना कर आसानी से कामयाबी हासिल की जा सकती है, इसका चयन भी सर्वप्रथम अत्यावश्यक है। अब और कंफ्यूज रहने की जरुरत नही है आज ही संपर्क करे 9871949259 से, हम आपको आपके जन्मजात प्रतिभा के आधार पर हम आपको करियर विकल्प देंगे जिसमें आप शीर्ष तक पहुँच सके ।
करियर सम्बंधित सलाह सुझाव के लिए इमेल करे anandmohan.dmt@gmail.com
अतः आइये हम सब साथ मिलकर संकल्प ले की आज के बाद हम अपने सम्पर्क के हर बच्चे को उसके मानसिक क्षमता के आधार पर ही अपने शिक्षा क्षेत्र के चुनाव करने का बहुमूल्य सुझाव देंगे I
जानवरों की तरह बच्चों के पीछे पड़ने से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है| इसलिए शिक्षा का स्वरुप बच्चो के दिमागी क्षमाताओ के अनुसार होना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियों को अपने सही दिशा की ओर अधिक से अधिक बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें| शिक्षा प्राप्त करने पर सुविधा प्राप्त होती है तथा में प्रसन्नचित्त होने के कारण जो भी शिक्षा ग्रहण करता है, वह उसके भावी जीवन को प्रसन्नचित्त रखकर जीने का अधिकार देती है| इस तरह विद्यार्थी में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता तथा छात्र एवं पालको के मध्य सामंजस्य होने के कारण शिक्षा का भावी रूप दिखाई देने लगता है I
मित्रो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को एक नयी विचारधारा, नया सवेरा देता है, ये हमे एक परिपक्व समाज और स्वर्णिम राष्ट्र बनाने में मदद करता है । यदि शिक्षा के उद्देश्य सही दिशा मे हों तो ये इन्सान को नये नये प्रयोग करने के लिये उत्साहित करते हैं । शिक्षा और संस्कार साथ साथ चलते हैं, या कहा जाये तो एक दूसरे के पूरक हैं । शिक्षा हमें संस्कारों को समझने और बदलती सामाजिक परिस्थियों के अनुरूप उनका अनुसरण करने की समझ देता है । आज शिक्षा जिस मुकाम पर पहुँच चुकी है वहाँ उसमें परिवर्तन की गुंन्जाइश है, आज हमें मिल बैठकर सोचना चाहिये, कि यदि शिक्षा हमारे उद्देश्यों को पूरा नही करती तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है ।
कैरियर के चुनाव मे उधेड़बुन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। फैसला बिल्कुल अपने लक्ष्य को केन्द्र में लेकर होना चाहिए। यदि आई.ए.एस. बनना है तो अपको किस रूचि के विषय को अपना कर आसानी से कामयाबी हासिल की जा सकती है, इसका चयन भी सर्वप्रथम अत्यावश्यक है। अब और कंफ्यूज रहने की जरुरत नही है आज ही संपर्क करे 9871949259 से, हम आपको आपके जन्मजात प्रतिभा के आधार पर हम आपको करियर विकल्प देंगे जिसमें आप शीर्ष तक पहुँच सके ।
करियर सम्बंधित सलाह सुझाव के लिए इमेल करे anandmohan.dmt@gmail.com
अतः आइये हम सब साथ मिलकर संकल्प ले की आज के बाद हम अपने सम्पर्क के हर बच्चे को उसके मानसिक क्षमता के आधार पर ही अपने शिक्षा क्षेत्र के चुनाव करने का बहुमूल्य सुझाव देंगे I